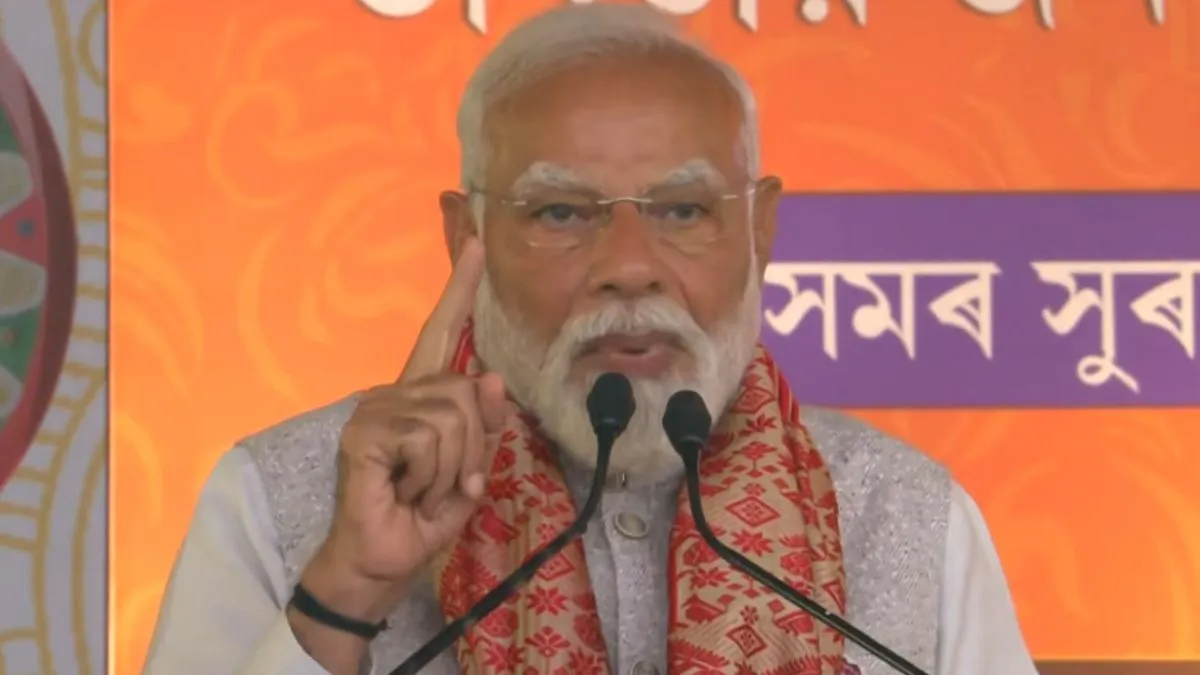(बॉलीवुड के अनकहे किस्से) गायकी और जयराज

1931 में आई फिल्म ‘आलमआरा’ के द्वारा भारत में बोलती फिल्मों का युग शुरू हुआ । मूक फिल्मों में कलाकारों का खूबसूरत होना ही काफी था, लेकिन अब खूबसूरती के साथ-साथ उसकी आवाज भी महत्वपूर्ण हो गई। इसका विपरीत असर फिल्मोद्योग के अनपढ़ एवं ऐंग्लो-इंडियन कलाकारों पर पड़ा। जयराज भी इस आंधी से बच नहीं सके। वे शारदा फिल्म कंपनी में थे और कंपनी ने ‘सस्सी-पुन्नू’ फिल्म के जरिए सवाक् फिल्म-निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा था। इसका नतीजा वही हुआ, जो होना था। मूक फिल्मों के कलाकारों की छुट्टी कर दी गई। इस प्रकार जयराज भी शारदा से बाहर हो गए।
सवाक् फिल्मों में गायक-नायकों की बहुत मांग थी। मा. निसार, अशरफ खान, मारुतिराव पहलवान, गोविंदराव टेंबे, फिरोज दस्तूर, पटवर्धन, कृष्णराव गोरे आदि गायक-नायक सवाक् फिल्मों के प्रारंभिक दिनों में छाये रहे। बेसुरे कलाकारों को उन दिनों कोई नहीं पूछता था। जाहिर है कि जयराज पर भी यह गाज गिरी। शारदा फिल्म कंपनी उन्हें सिर्फ एक सौ पच्चीस रुपये देती थी। इनमें से साठ रुपये देकर वे नागेंद्र मजूमदार के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे। नागेंद्र मजूमदार मूक फिल्मों में जयराज के निर्देशक थे, शारदा फिल्म कंपनी ने उनकी छुट्टी कर दी, तो मजूमदार ने भी उन्हें घर से बेघर कर दिया।
मजबूरन उन्हें परेल में एक कमरा किराये पर लेना पड़ा । फिर भी रोजी-रोटी की समस्या तो थी ही। गायक-नायकों की इस होड़ में शामिल होना है तो गायन सीखना ही पड़ेगा यह बात अच्छी तरह से समझकर जयराज एक उस्ताद से गायन के पाठ सीखने लगे। उनके गायन सीखने के पूरे रोचक प्रकरण को उस समय के प्रख्यात मराठी फिल्म पत्रकार इसाक मुजावर ने लिखा था और उसका प्रकाश भात्मब्रेकर द्वारा किया गया। हिंदी अनुवाद सारंगा स्वर नामक पत्रिका ने प्रकाशित किया था। उसके अनुसार जयराज ने एक हारमोनियम भी खरीद लिया। उन दिनों सिर्फ बीस रुपये में हारमोनियम मिल जाता था।
हफ्ते में दो दिन उस्ताद उन्हें तालीम देने आते थे। बाकी दिनों वे पूरी तन्मयता से रियाज किया करते थे। चाल में रहनेवाले पड़ोसी उनके गाने-बजाने से हमेशा नाराज रहते थे। फिर भी जयराज को कोई चिंता नहीं थी। वे हर हालत में गायन सीखने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे। पच्चीस रुपये महीना देकर वे उस्ताद से गाना सीख रहे थे। इसके अलावा तबलची को भी ग्यारह रुपये देने पड़ते थे। पूरे चार महीने वे इस चक्कर में उलझे रहे। पर कोई फायदा नहीं हुआ।
एक दिन थक हारकर उनके उस्ताद ने उनसे कहा, “बेटा, तुम्हारी आवाज में गहराई तो है, पर वह सुरीली नहीं है।” उस्ताद के मुंह से यह टिप्पणी सुनकर उनका दिल खट्टा हो गया। फिल्मोद्योग में उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। इस बीच हैदराबाद की ईस्टर्न फिल्म्स ने ‘शिकारी’ तथा ‘गुलशन-ए-हवस’ नाम से हिंदी-अंग्रेजी फिल्म की योजना बनाई थी। बी.आर. देवधर इसका संगीत निर्देशन करनेवाले थे। इसका नायक बौद्ध भिक्षु था। चूंकि फिल्म दो भाषाओं में बन रही थी, उसमें ऐसा नायक चाहिए था जो हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में माहिर हो।
इस भूमिका के लिए जयराज की सिफारिश देवधर पहले ही कर चुके थे। लेकिन भूमिका महत्वपूर्ण होने से केवल सिफारिश के आधार पर नायक का चयन संभव नहीं था। चयन के लिए ‘ऑडिशन टेस्ट’ सबसे पहली अनिवार्यता थी। जयराज ने इस कसौटी से पार पाने की ज़ोरदार तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पूरा गालिब रट लिया। हिंदी-उर्दू उच्चारणों का भरपूर अभ्यास किया। साथ ही अंग्रेजी का अभ्यास भी जरूरी था। इसलिए बुद्धकालीन पृष्ठभूमि पर एडविन आर्नल्ड की लिखी पुस्तक ‘लाइट ऑफ एशिया’ का एक उद्धरण भी उन्होंने रट लिया।
बंबई के कोलाबा में मोंगिनीज होटल में यह ऑडिशन टेस्ट होने वाला था। फिल्म के लेखक थे मुंशी हिल और निर्देशक थे केवल गांधी। जयराज पूरी तैयारी के साथ गए थे। सवाक् फिल्मों की अंधेरी गुफा में अवसर ढूंढ़ने के लिए जयराज के और भी कई साथी वहां आए थे। इनमें डी. विलीमोरिया भी शामिल थे। उच्च शिक्षित होने के कारण जयराज का उच्चारण शुद्ध था। इसके अलावा मानसिक रूप से भी वे इस अग्निपरीक्षा के लिए तैयार थे। फिर तो जयराज का चयन होना ही था। इस फिल्म में ऐंग्लो-इंडियन लड़की सीता देवी (रमी स्मिथ) जयराज की नायिका थी।
इसके अलावा जगदीश सेठी, जाल खंबाटा, शहजादी बानू आदि की प्रमुख भूमिकाएं थीं। इस फिल्म के लिए तीन महीने की अवधि तक तीन सौ रुपये माहवार पर जयराज को अनुबंधित किया गया। हैदराबाद में ही इस फिल्म की पूरी शूटिंग की जानी थी। बुद्धकालीन वातावरण बनाने के लिए वहां एक पूरा गांव ही बसाया गया था। अंग्रेजी-हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ इस फिल्म का फिल्मांकन हुआ था। लेकिन इसका अंग्रेजी संस्करण कमी परदे पर आया ही नहीं। हां, धोबी तालाब इलाके के वेलिंग्टन हॉल में यह हिंदी फिल्म जरूर प्रदर्शित हुई थी।
इस हिंदी फिल्म को परदे पर दिखाने से पहले उसमें जोहरा मुस्तरी के कुछ गीत शामिल किए गए थे। यह फिल्म बहुत ज्यादा सफल भले ही न रही हो, पर फ्लाप भी नहीं हुई थी। यहीं से सवाक् फिल्मों में जयराज का सिलसिला शुरू हुआ। गायकी के बिना उन्हें वहां प्रवेश मिल गया था। क्योंकि बौद्ध भिक्षु का गाने से भला क्या वास्ता? लेकिन इसके बाद ‘पतित पावन’, ‘अहिल्योद्धार’ फिल्म में जो भूमिका उन्हें मिली उसमें गाने से बचना मुश्किल था। यह फिल्म ‘प्रतिमा फोटोटोन’ की पेशकश थी।
जयराज की भूमिका वाली कई मूक फिल्मों का निर्देशन नागेंद्र मजूमदार ने किया था। उन्हीं की बदौलत जयराज को यह भूमिका भी मिली थी। इस फिल्म में उनकी नायिका थीं दुर्गा खोटे । प्रभात की फिल्म ‘अयोध्येचा राजा’ में सफल अभिनय के बाद गायिका अभिनेत्री के रूप में वे प्रतिष्ठित हुई थीं। इसके संगीत निर्देशक प्रो. बी. आर. देवधर ही थे। उन्हें मालूम था कि गाना जयराज के बस का नहीं है। उन्होंने ‘पतित पावन’ के एक गाने का पूरे एक महीने तक उनसे रिहर्सल करवाया। आश्रम के एक सेट पर इस गाने को फिल्माया जाना था। इसके लिए विरार में आश्रम का सेट बनवाया गया था। उन दिनों प्ले-बैक पद्धति प्रचलित नहीं थी। इसलिए कैमरे के सामने गाने के साथ-साथ अभिनय करना लाजिमी था।
इस फिल्म के कैमरामैन थे रजनी पंड्या। उन्होंने इस गाने का फिल्मांकन शुरू किया। तबलची और बाजे वाले को ट्राली पर बिठा दिया गया। ट्राली के गतिमान होने के साथ ही बजवैये भी आगे-पीछे हो जाते थे। इस पूरी जोड़-तोड़ में गायक-वादकों में कोई तालमेल नहीं रहता था। इस स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से साजिंदों को जयराज के कदमों में बिठलाया गया। इसके परिणामस्वरूप साजिद भी कैमरे की गिरफ्त में आने लगे। अतएव घुटने के ऊपर के हिस्से को ही कैमरे को फोकस में रखकर जैसे-तैसे उस गाने का फिल्मांकन पूरा कर लिया गया।