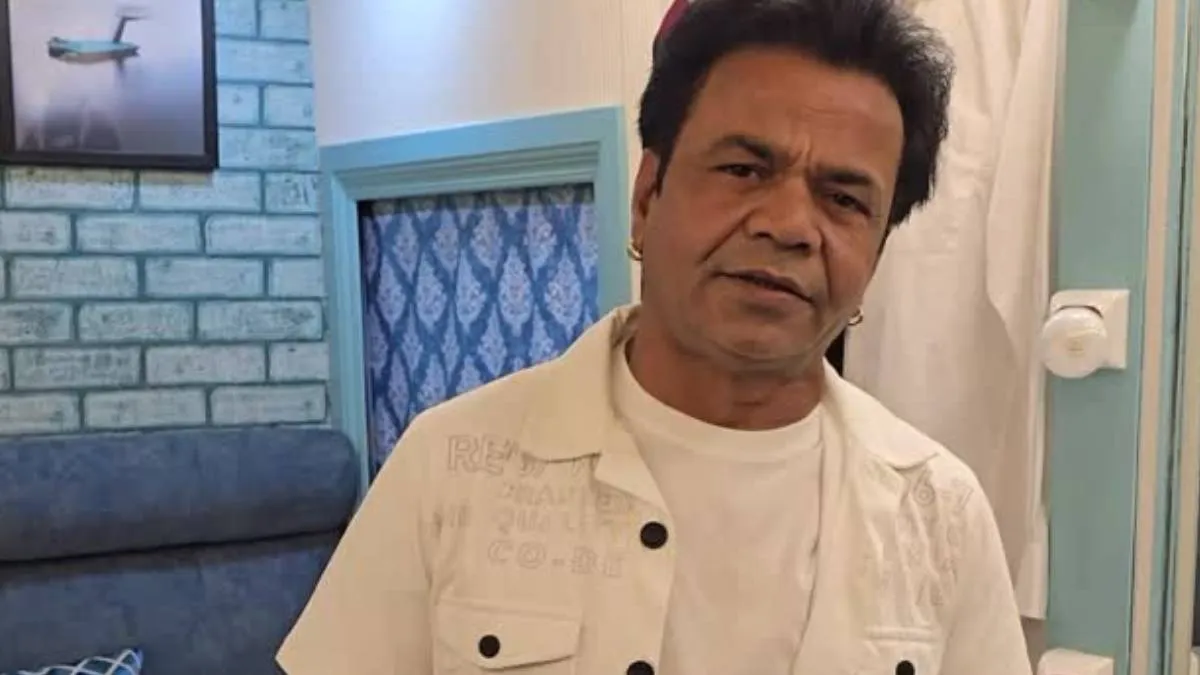भारत की आत्मा को पहचानने की जरूरत

‘भारत’ और उसके सत्व या गुण-धर्म रूप ‘भारतीयता’ के स्वभाव को समझने की चेष्टा यथातथ्य वर्णन के साथ ही वांछित या आदर्श स्थिति का निरूपण भी हो जाती है। भारतीयता एक मनोदशा भी है। उसे समझने के लिए हमें भारतीय मानस को समझना होगा । यह सिर्फ ज्ञान का ही नहीं बल्कि भावना का भी प्रश्न है और इसमें जड़ों की भी तलाश सम्मिलित है। आज इस उपक्रम के लिए कई विचार-दृष्टियां उपलब्ध हैं जिनमें पाश्चात्य ज्ञान-जन्य दृष्टि निश्चित रूप से प्रबल है जिसने औपनिवेशिक अवधि में एक आईने का निर्माण किया जो राजनैतिक–आर्थिक वर्चस्व के साथ लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो गया यद्यपि उसके पूर्वाग्रह दूषित करने वाले रहे हैं । उसकी बनाई छवि या आत्मबोध ने एक इबारत गढ़ी जो औपनिवेशिक शिक्षा द्वारा आत्मसात् कराई गई। इस क्रम में अंग्रेजी राज का ‘अन्य’ भारतीय जनों द्वारा ‘आत्म’ के रूप में अंगीकार किया गया । वेश-भूषा, राज-काज और बात–व्यवहार में अंग्रेजियत आभिजात्य और श्रेष्ठ होने का असंदिग्ध पर्याय और देसी (भारतीय!) दोयम दर्जे का बना दिया गया। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बना दिया और हमने भी संविधान में वैसे ही दर्ज किया–इंडिया दैट इज भारत !
भारत और भारतीयता-विमर्श की चुनौती तब सचमुच और कठिन हो जाती है जब हम इस वैचारिक परियोजना को देश और काल के ठोस यथार्थ के धरातल पर आयोजित करते हैं और भारत की अपनी देशज दृष्टि से आगे बढ़ते हैं । यह भारत-दृष्टि एक देशज दृष्टि है – एक अतिक्रामी दृष्टि है जो ‘मैं’ और ‘तुम’ की कोटियों से ऊपर उठ कर समग्र सृष्टि को समेटने वाली है। साकल्य, जीवन की पूर्णता, क़र्म की भावना, समष्टि की उन्नति और भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बोध से समन्वित इस व्यापक विचार-परियोजना की कई सीमाएं हैं। किसी प्रत्ययविशेष का दिक्कालातीत (या कहें शाश्वत!) निरूपण अमूर्त जगत में जिस निर्बंध विचरण की अपेक्षा करता है जिसे अनिर्वचनीयता असहज नहीं करती है। यह एक अतिरिक्त सीमा हो जाती है ।
आज के यथार्थ के अति आग्रही कालखंड के दौर में यह सोच खामखयाली है, अचिंत्य है और सामान्यतया ग्राह्य ही नहीं है । अब निरवधि काल की चेतना को प्रायः निरस्त सा करते हुए सामान्य जन, विज्ञान के सावधि और तत्काल इंद्रियानुभवगम्य प्रत्यक्ष तक ही अपने को सीमित-संकुचित करते जा रहे हैं । तात्कालिकता के घोर दबाव तले अपने को बरतने की मजबूरी कुछ ऐसी होती जा रही है कि आंख की ओट वाला (अव्यक्त!) सब कुछ प्रश्नांकित और संदिग्ध होता जा रहा है। व्यवहार को मात्र सद्य: व्यक्त क्षण में ही स्थापित करने की तीव्रतर होती आकांक्षाओं के प्रति समर्पण करते हुए हम सत्य, यथार्थ और अस्तित्व के अनुभव-प्रामाण्य के तर्क तक ही अपने विमर्श को समेटते जा रहे हैं। यह अवश्य है कि हमारे आशय, अभीष्ट और उद्देश्य-यानी वह सब कुछ जो रोचक, सार्थक और निरंतर को जन्म देता है या दे सकता है- इस स्वतः आरोपित लौकिक परिधि को खंडित करते हुए हमें अनुमान की दुनिया में ले जाने वाला है। यह अज्ञात और अपरिचित होने पर भी ‘संभव’ को अर्थात् भविष्य को व्यंजित करता है । वैसे भी शब्द (प्रतीक) का अर्थ उसकी लोक-व्याप्ति में ही परिलक्षित और गृहीत होता है !
वस्तुतः विचार और वास्तविक सत्य (आब्जेक्टिव रीएलिटी) या अमूर्त और मूर्त की कोटियां एक-दूसरे को स्पर्श करती और गढ़ती हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य बहुत हद तक कामचलाऊ भेद हैं जो देश काल के भीतर समकालीन अवस्थिति के साथ अनिवार्यत: बनते बिगड़ते रहते हैं। भविष्य क्रमश: वर्तमान होता जाता है और वर्तमान भूत में तब्दील होने को तत्पर रहता है। यह भी ध्यातव्य है कि वाचिक परम्परा से आगे और उसके ह्रास के साथ अब सांप्रतिक परिदृश्य में बौद्धिक संकल्प और तकनीकी सहयोग न केवल इनकी प्रस्तुति (रिप्रेजेंटेशन) तय करते हैं बल्कि इन तक हमारी पहुंच (एक्सेस) को घटाते-बढ़ाते रहते हैं और पुनरीक्षण (तथा कृत्रिम बुद्धि की सहायता से ) पुनर्रचना का भी अवसर देते हैं ।
साथ ही वे अवसरानुकूल अपने हितसिद्धि के लिए सामग्री को ‘क्लैसीफायड डाक्कूमेंट’ कह कर (सीमित अवधि या सदैव के लिए) प्रतिबंधित भी करते हैं । अतः आज के युग में हमारी अनुबंधित नियति हो गई है कि हम स्वयं को सतत आविष्कृत, परिभाषित और परिसीमित करते रहें और उसे अपने और दूसरों के लिए सतत प्रमाणित और प्रचारित भी करते रहें। स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए भी इस तरह का उद्यम सामाजिक अस्तित्व की एक अनिवार्यता सी हो रही है । कहना न होगा कि सांस्कृतिक परम्परा का संवर्धन इसी प्रकार के ज्ञान-आख्यान की प्रचलित प्रथाओं के अंतर्गत होने लगा है जिसे आंतरिक (स्थानीय!) और बाह्य (वैश्विक!) (अधिकृत) शक्तियां संयोजित (और प्रायोजित!) करती हैं। पेटेंट के दौर में यह स्पष्टतः एक तरह की खरीद-फरोख्त जैसी प्रक्रिया होती जा रही है। अब ज्ञान से मुक्ति की कामना – सा विद्या या विमुक्तये – (इमेंसिपेशन) निरपेक्ष न हो कर सशर्त ही संभव है।
भारतीयता की अवधारणा ‘भारत’ से अविभाज्य रूप से सम्पृक्त है जो निश्चय ही पृथ्वी का एक भू-भाग भी है पर वह भू–भाग मात्र ही नहीं है। भारतीयों के लिए वह मुख्यतः विचार तथा भाव का पवित्र विषय है । वह हमारी चेतना या सांस्कृतिक आत्मबोध का नियामक एक प्राथमिक अंश है । स्वाभाविक है भारत की स्थिति, प्रतीति और अनुभूति का सत्य निरपेक्ष और अर्थशून्य न हो कर द्रष्टा, प्रेक्षक और भावक की पृष्ठभूमि यानी वैचारिक तैयारी और संलग्नता पर ही निर्भर करेगा। मनुष्य की वाचिक ढंग की प्राचीनतम रचना ‘वेद’ के समय से ही भारत वसुंधरा की छवि जीवनदायिनी माता के रूप में संकल्पित की जाती रही है। हाड़ मास का बच्चा माता के शरीर से निर्मित होता है, गर्भ में उसके रक्त से पलता है, आकार पाता है और जन्म के उपरांत उसके दूध के आहार पर जीता है। माता की उपस्थिति संतति की अपरिहार्यता है।
यद्यपि माता और संतति के मध्य का यह स्वाभाविक सम्बन्ध एक चिरंतन सत्य है और तादात्मीकरण का सहज आधार बनाता है तथापि इस सम्बन्ध को व्यापक सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक परिवेश न्यस्त रुचि और लाभ के मद्देनज़र भिन्न-भिन्न अर्थ देता रहता है। फलतः विभिन्न काल खंडों में सामाजिक यथार्थ और सामाजिक स्मृति के रूप में अस्मिता-निर्मिति अलग-अलग रूप लेती रहती है या कि उसके अलग-अलग पक्षों पर बल दिया जाता रहा है । ऐसे में भिन्न-भिन्न प्रेरणाएं उदित और अस्त होती रही हैं। कुछ भू-क्षेत्रों में समाज के स्तर पर विशिष्ट प्रवृत्तियां भी परिलक्षित हुई हैं। विश्व-पटल पर दृष्टिपात करें तो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी और हिंसा तथा शोषण को प्रश्रय देने की प्रवृत्ति का कुछ क्षेत्रों में बाहुल्य इस परिघटना का प्रमाण देते आ रहे है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सभ्यता और संस्कृति की सतत प्रवहमान मानवी गाथा में अनेक प्रवृत्तियों का संघात मिलता है। इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही धाराओं को आकार मिलता रहा है।
इतिहास की नब्ज थामे गुरुदेव रबीन्द्र नाथ टैगोर ‘भिन्न के योग में निहित छंद’ और ‘ताल बचा कर समय तक पहुंचने’ को मनुष्यत्व का निकष घोषित करते हैं। भारतीय इतिहास का आरंभ आर्य–अनार्य के जाति संघर्ष की कथा के साथ ग्रहण करते हुए वे भारतीय महाकाव्यों का सर्जनात्मक सामाजिक-ऐतिहासिक विचार करते हैं। वे आर्य–अनार्य सभ्यता के बीच संघर्ष और रामचंद्र की विजय का रोचक विश्लेषण करते हैं। वे भागवत इतिहास और पुरातन-नूतन का विरोध का सम्यक विचार करते हैं। उनकी दृष्टि में ‘जातियों के संघात से आत्म-प्रसारण की जगह आत्म-रक्षा की वृत्ति’ बलवान हुई। उनकी दृष्टि में आर्य–अनार्य का चिंतन सम्मिश्रण सौंदर्य के उदय का कारण बना। गुरुदेव का सूत्र वाक्य है – ”बहुत्व के बीच अपने आपको बिखराना भारत वर्ष का स्वभाव नहीं है। वह ‘ए’ को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए बाहुल्य को एकत्र में संयत करना ही उसकी साधना है । भारत की अंतरतम सत्य प्रकृति स्वयं उसे निरर्थक बहुत्व के भीषण योग से बचाएगी।” गुरुदेव अंतरराष्ट्रीयता पर भी टिप्पणी करते हैं, ”अपने को त्याग करके दूसरों की चाहना जिस तरह निष्फल भिक्षुकता है, उसी तरह दूसरों का त्याग करके अपने को संकुचित करना दारिद्र्य है, चरम दुर्गति है।” उनकी राय में अपने देश में सर्वदेशों को और सर्वदेशों के बीच ही अपने देश को सत्य के रूप में पाया जा सकता है।